दुर्दिनों की बारिश में रंग: कविता संग्रह / मणि मोहन मेहता
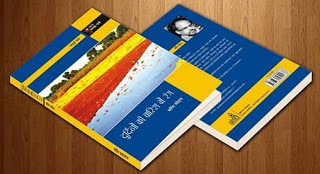 "अपने छोटे संसार में जहाँ यह सब पाषाणकालीन मौलिकता में जीवित है, वहाँ से इन कविताओं का फूटना..."
"अपने छोटे संसार में जहाँ यह सब पाषाणकालीन मौलिकता में जीवित है, वहाँ से इन कविताओं का फूटना..."
ज़िन्दगी को सजीव कर देती हैं कविताएँ। जिस ‘कम्फर्ट जोन’ में आदमी ने अपना नया जीवन तलाश लिया है और जिसे अपना पूरा संसार मान लिया है, उसे एक झटके में निरर्थक कर देती हैं। इस नए कम्फर्ट जोन पीले पत्ते गिरकर मिटटी के रंग के नहीं होते, किचन की स्लैब से बर्तन गिरने की आवाजें नहीं होतीं और होती भी हैं तो किताब में मग्न आदमी के ज़हन में बर्तन के नाम का अनुमान तो हरगिज़ नहीं होता; इस कम्फर्ट जोन में घरों की छतों पर अपने नीड़ों में वापसी करते परिंदों की परछाइयाँ नहीं गिरतीं। इस कम्फर्ट जोन के घरों पर तो छतें तक नहीं होतीं।
ये कविताएँ उस दिनचर्या से उपजी हैं जिसने हर पिघलते दिन के साथ इनके जीवंत एहसास को जिया है; घर लौटते हुए अपनी पत्नी के लिए वेणी और बेटी के लिए आइसक्रीम खरीदी है। अगर कवि उन तथाकथित ‘मशरूफ’ शहरों में रहता और यही विषय रहे होते तो अनुमान लगाना सहज है कि इन कविताओं का शून्य और गहरा होता, रंग और चटख होते, व्याकुलता और मार्मिक होती। इन ‘मशरूफ’ शहरों में रहने वाले लोग शाम को घरों की ओर चलते ज़रूर हैं पर कितने लौट पाते हैं पता नहीं।
अपने छोटे संसार में जहाँ यह सब पाषाणकालीन मौलिकता में जीवित है, वहाँ से इन कविताओं का फूटना कवि की मौलिकता और उसकी गहरी जड़ों का, उसके कुलबुलाते मन मस्तिष्क का, प्रश्न उठाने के साहस का, बूँद भर पानी से तृप्त हो जाने के संतोष का, लुप्तप्राय हो चले आम आदमी के खुद में मग्न रहने के पागलपन का, मिट्टी के आशीर्वाद का, परिवार को प्रसन्नता देने की उपलब्धियों का, चीटियों और गिलहरियों के साथ सुख-दुःख बाँटने के सौभाग्य का, किताबों की जिरह में हार जाने के मर्म का, शब्दों को कैद रखने के प्रायश्चित का और फिर उन्हें स्वतंत्र कर देने के उल्लास का.....गहन परिचायक है।
पन्ने करीब-करीब सब पलटे जा चुके हैं। शब्दों के मायने साथ-साथ ज़हन में तैरने लगे हैं, अंत में पाया कि एक भी शब्द कठिन नहीं था, न नया था कि गूगल से व्याख्या मांगने की ज़रुरत पड़े। इन साधारण से शब्दों के ज़रिये एक साधारण सी लगने वाली यात्रा में कुछ असाधारण पड़ाव हैं। एक कविता कभी अर्धविराम की तरह ख़त्म होती है और कहती है ‘तुम खुद सोचो’। कुछ पूर्ण विराम हैं जो कहते हैं ‘ये साधारण किन्तु स्थापित तर्क है, सोचना समय की बर्बादी है’। इन्हीं साधारण से शब्दों और उनमें बिंधी हुई भाषा को बचाने की और इस भाषा से उपजी कविता को अमृत्व देने की जिजीविषा एक सतत परछाईं की तरह हर पूर्णविराम में दिखाई देती है। वह फिर चाहे ‘डंपिंग ग्राउंड’ से ‘किसी तानाशाह की जी हुजूरी अभिनन्दन के बाद ज़हन में बची रह गयी भाषा’ हो, ‘इंतज़ार’ में ‘किसी दिन डाल दूँगा एक कटोरी आटे के साथ अपनी थोड़ी सी भाषा भी’, ‘कविता’ में बहते हुए पसीने और लुढ़कते हुए आंसुओं के साथ ‘कभी-कभी ऐसे ही आ जाती है कविता की भाषा भी होठों तक’, ‘अब और नहीं’ में ‘आपको पता नहीं इस वक़्त किस कदर बेचैन है कविता मेरे करीब आने के लिए’, ‘शरणार्थी शिविर’ में ‘अपने सिर पर बचे-खुचे अर्थ की गठरी उठाए कुछ शब्द आए’, ‘शायद’ के अलग मायने उभर कर आते हैं जब कवि कहता है ‘भाषा के आसमान का यह टूटा हुआ सितारा है....’ और ‘दुनिया की तमाम भाषाओं के अन्धकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता-चमकता’, और अंत में ओ हेनरी की ‘लास्ट लीफ’ के गहरे हरे रंग के पत्ते में जड़ दिया भाषा का यह नगीना ‘यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फवारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है आइवि की लता से गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर’, ‘घर’ में ‘अब बस घर चाहिए उन्हें, माँ चाहिए, हवा में उछलती गेंद की तरह, जानी पहचानी भाषा चाहिए’।
इन कविताओं में रिश्ते हैं... ‘एक दिन’ में ‘अपनी नम आँखों से मेरी तरफ देखते हुए तुम जिद करोगी वहाँ चलने की और मैं कहूँगा-उड़ सकोगी इतने प्रकाश वर्ष दूर’, ‘कन्फैशन’ में ‘छतरी की तरह बनी रही सिर पर दुर्दिनों की बारिश में बीसियों बार’, ‘पिता के लिए’ में ‘कहाँ दे पाया इतना प्यार बच्चों को जितना मिला मुझे अपने पिता से’, कई बार यह मन में गुजरा कि मैं पिता की तरह कैसा हूँ, कम से कम अपने पिता की तुलना में। ‘बाप बनकर तेरे करीने से लेटता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ, मैं बेटा बुरा था या बाप बुरा हूँ’। अच्छा है कि यह सवाल उठता है...उठता रहे। ‘बेटी’ में भी मुझे अपनी एक कविता का अक्स गहराई से नज़र आता है जब कवि कहता है ‘ज़रा सी आहट पर भागती है बेटी घर का दरवाजा खोलने के लिए’। एक निजी अनुभव से जन्मी उस कविता की अनुगूंज यहाँ भी सुनाई देती है ‘और यह कमबख्त दरवाजा भी अपने आप नहीं खुलेगा’। मेरी पत्नी की पहली प्रेगनेंसी थी जो हमें टर्मिनेट करानी पड़ी क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं थी। हम लोग बेटी की उम्मीद कर रहे थे। तब लिखी थी यह कविता ‘तू मेरे घर जरूर आई होगी, मैंने ही दरवाजा न खोला होगा। थक जाता हूँ, दफ्तर से आकर सो गया हूँगा और तेरी माँ भी दिन भर की थकी अलसाई होगी... तू मेरे घर जरूर आई होगी।’
प्रकृति है....‘रूपांतरण’ में ‘कितनी ख़ामोशी के साथ हो रहा है प्रकृति में रंगों का यह रूपांतरण’, ‘फूल’ में भी प्रकृति और दर्शन का प्रभावी संगम देखने को मिलता है ‘दिन निकलते ही आ बैठती है धूप, तितली, भंवरे, मधुमक्खी, दिन भर लगा रहता है किसी न किसी का आना-जाना..फूलों को पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है दिन और करीब आ जाती है शाम....जिसकी बाहों में उसे टूटकर बिखरना है’। पशु हैं... जो प्रकृति और कवि में एकाकार हो गए हैं। ‘अपना हिस्सा’ में ‘मुझे सिर्फ बादल के कुछ पहाड़, शेर, भालू, हाथी, बादल के कुछ टुकड़े दे दो’, ‘अफ़सोस’ में तोते, बिल्ली और कुत्ते के माध्यम से मनुष्य के दुर्व्यवहार को रेखांकित किया है जो सराहनीय है। ‘बिल्ली’ में मनुष्य की बुद्धिमत्ता को धराशाई कर देने वाला चित्रण है जो कवि की डिग्रियों के वर्णन से प्रभावी बन गया है. ‘और एक हम हैं ढपोर शंख, एम ए, एम फिल, पी एच डी’। करीब दस पंद्रह साल तो ज़रोर्र गुजर गए होंगे ‘ढपोर शंख’ को पढ़े या इस्तेमाल किए हुए। इस शब्द को पुनर्जीवित करने के लिए आभार।
दर्शन है...‘अलाव’ में ‘उसे रुकने के लिए पुकारती ही रह गई अलाव की आग’, ‘मिटटी’ में ‘मिटटी से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है इस संसार में’, ‘दुःख’ में फलसफा है ‘अब इतनी सी बात पर क्या उठा कर फेंक दें अन्न से भरी थाली, क्या इतनी सी बात पर देने लगें ज़िन्दगी को गाली’।
इन सब के अतिरिक्त ‘प्रेम गीत’ और ‘एकालाप’ में छोटी पर बेहद आकर्षक पंक्तियाँ हैं। संग्रह के अंत में ये वैसे ही पेश आती हैं जैसे छप्पन भोग खाने के बाद स्वादिष्ट मुखवास।
एक परिपूर्ण कविता संग्रह है जो न्यौता सा देता है कि यदि जीवन में सामंजस्य बनाए रखना है तो कौन से अवयवों की कितनी मात्र होनी चाहिए। जमीन से जुड़े हुए लोगों के जीवंत सन्देश हैं जो आशा है कि ‘मशरूफ’ लोगों के ज़हनों में पहुँचें। कुछ विचार फिसल गए हैं लिखते-लिखते। कभी याद आए तो मना कर भेज दूँगा। मणि भाई को हार्दिक बधाईयाँ। फेसबुक पर उनकी कविताओं और उनके अनुवादों से रू-ब-रू होते रहते हैं। बहुत कुछ सीखने और मनन करने को मिलता है। प्रार्थना है कि ये सफ़र इसी तन्मयता से जारी रहे। मधुमक्खियों, गिलहरियों, चींटियों और बेटियों को जीवन मिलता रहे, पुनर्चक्रण होता रहे। वरना आदमी को खुद कहाँ पता है कि वह क्या कमाने निकला था।
Published on July 02, 2017 01:20
No comments have been added yet.



